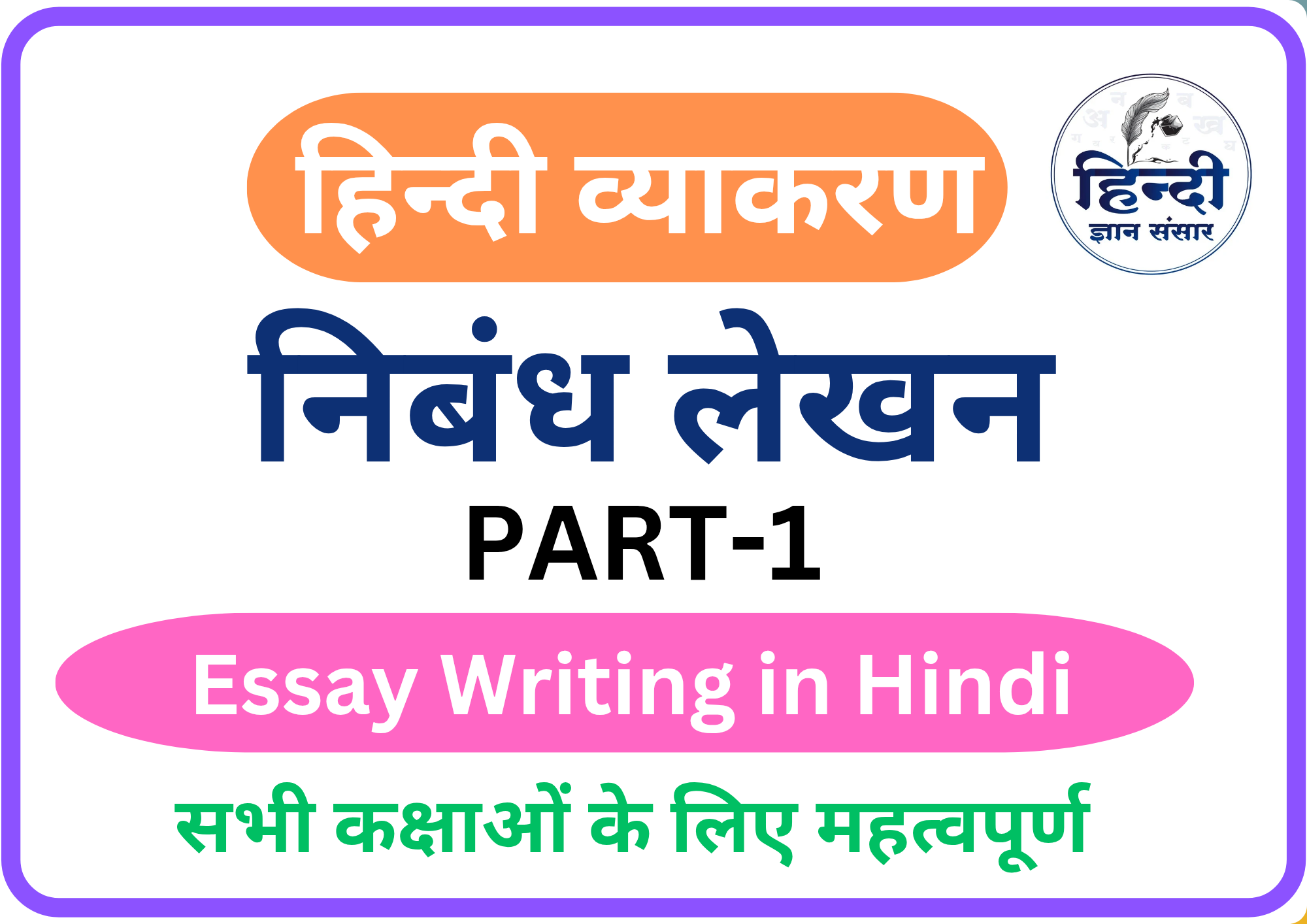
इस लेख में हम निबंध लेखन Class 12 के बारे में जानेंगे। निबंध लेखन हिन्दी में से राजस्थान बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। परीक्षा में Essay writing in Hindi का शीर्षक देकर निबंध लेखन करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इस लेख में निबंध लेखन की परिभाषा, निबंध लेखन के प्रकार आदि का अध्ययन करेंगे।
निबंध लेखन गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। अन्य गद्य विधाओं कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावृत्तांत आदि में निबंध लेखन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार – ‘निबंध गद्य की कसौटी है।’
संस्कृत साहित्य में महाकवि दण्डी की उक्ति है – “गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति।” अर्थात ” कवि की कसौटी कविता नहीं बल्कि गद्य है।
निबंध रचना में गद्य का उत्कृष्ट रूप व्यक्त होता है एवं यह मन के भावों, विचारों की से स्पष्ट व्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है।
निबंध का शब्द का अर्थ होता है – निश्चित बंध।
बंध का मतलब होता है – भली प्रकार से बंधी हुई रचना। व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को एक सूत्र में बांधता है।
“व्यक्ति द्वारा लिखित वह रचना जिसमें अपने मन के भावों और विचारों को क्रमानुसार लिपिबद्ध किया गया हो, उसे निबंध कहते हैं।”
अंग्रेजी में निबंध को Essay कहते हैं जिसका अर्थ होता है – प्रयत्न।
बाबू गुलाब राय ने निबंध के बारे में कहा है कि “निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकर के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक निजीपन स्वच्छंदता स्वास्थ्य सचिव था तथा आवश्यक संगती एवं संबद्धता के साथ किया गया हो।”
( निबंध लेखन हिन्दी)
निबंध के मुख्य रूप से तीन तत्व माने गए हैं ।
1. निबंध की भाषा – निबंध में वह भाषा जो व्याकरण सम्मत परिष्कृत और शुद्ध रूप से लिखी गई हो तथा जिसमें पाठकों को प्रभावित करने की और विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण क्षमता हो।
2. निबंध के भाव एवं विचार – निबंध लेखन में भाव और विचारों की क्रमबद्ध, गंभीरतापूर्वक, प्रभावशाली और विषयानुरूप अभिव्यक्ति होनी चाहिए।
3. निबंध लेखन की शैली – निबंध की शैली साहित्यिक गुणों से संपन्न और निबंध के आकार के निजीपन को प्रकट करती है। शैली के अनेक भेद होते हैं लेकिन उसमें आकर्षण, सरसता व रोचकता होना जरूरी है।
(Rbse solution 12th class)
निबंध के निम्नलिखित भेद होते हैं
1. विचारपरक निबंध – इसमें निबंध को अपने विचार और कल्पना के आधार पर लिखा जाता है इसलिए ऐसे विचार परक लेखन कहते हैं। इस प्रकार के निबंधों में चिंतन को प्रमुखता दी जाती है। इसमें मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक निबंध इस श्रेणी में आते हैं।
2. वर्णनात्मक निबंध – किसी विषय वस्तु को वर्णनात्मक रूप में लिखना ही वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। इस प्रकार के निबंधों में प्राकृतिक दृश्य, मेला, उत्सव, तीर्थ स्थान, किसी ऋतु आदि का वर्णन किया जाता हैं।
3. विवरणात्मक निबंध – किसी पौराणिक, ऐतिहासिक, साहसपूर्ण घटना के वर्णन को विवरणात्मक निबंध कहते हैं। ऐसे निबंध युद्ध, यात्रा, जीवनी, साहसिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं आदि पर लिखे जाते हैं।
4. ललित निबंध – ऐसे निबंध जिनकी भाषा शैली, वाक्य रचना, मुहावरे, अलंकार आदि का प्रयोग करके भाषा सौंदर्य को समाहित किया जाता है, जिनको पढ़कर पाठक का मन प्रसन्न हो जाए, उन्हें ललित निबंध कहते हैं।
(Rbse solution 12th class)
1. शीर्षक :- निबंध का उचित और आकर्षक शीर्षक होना चाहिए। जिससे पाठक निबंध पढ़ने के लिए उत्सुक हो सकें। किसी परीक्षा में निबंध लेखन के लिए शीर्षक पहले से ही सवाल में दिया गया होता है। उस शीर्षक के आधार सारगर्भित विषयवस्तु के साथ निबंध का विस्तार किया जाता है।
2. प्रस्तावना – प्रस्तावना में निबंध की विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है जिससे पाठक को निबंध के अगले भागों को समझने में आसानी रहती है। जैसे विषय की परिभाषा, उससे संबंधित सूक्ति या कथन, उदाहरण, विवरण, उसकी महत्वता विवरण आदि प्रभावशाली होने चाहिए।
3. निबंध का विस्तार या प्रसार – निबंध के मध्य भाग में विषय वस्तु का बिंदुवार विवेचन और उसे संबंधित कथन का समावेश होना चाहिए। निबंध लेखन से पहले उससे संबंधित बिंदुओं को हमें rough work के रूप में तैयार कर लेना चाहिए। उन बिंदुओं के आधार पर उचित भाषा में निबंध का विस्तार करना चाहिए। निबंध के इस भाग में लेखक की योग्यता, उसकी कल्पना शक्ति और विचार की क्षमता का पता लगता है।
4. उपसंहार – यह निबंध लेखन के अंत में लिखा जाता है। उपसंगर में संपूर्ण निबंध का संक्षिप्त रूप होता है तथा उसके मुख्य बिंदु को बताया जाता है। उपसंहार सारगर्भित भाषा में लिखा होना चाहिए।
विद्यार्थियों को निबंध लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए –
1. सर्वप्रथम निबंध के शीर्षक पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए तथा उससे संबंधित सामग्री का संकलन करना चाहिए।इसके लिए उचित सूक्ति, कथन, मुहावरे , लोकोक्तियां आदि पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। जिनका निबंध का विस्तार करते समय उचित स्थान पर प्रयोग किया जाता है।
2. निबंध लेखन करने से पूर्व उसकी संक्षिप्त रूपरेखा बनाने चाहिए। उस रूपरेखा में प्रस्तावना, निबंध का मध्य भाग अर्थात प्रसार, उपसंहार आदि में दिए जाने वाले अपने मन के भाव और विचारों को शीर्षक में क्रमबद्ध रूप से रखकर लेखन करना चाहिए।
3. निबंध लेखन करते समय संकेत बिंदुओं के संक्षिप्त शीर्षक देकर उनके अनुसार उसके उपशीर्षक और अन्य बिंदुओं का विभाजन करना चाहिए।
4. अच्छे विचारों की पुष्टि के लिए कवियों के सुभाषित, सूक्ति और उनसे संबंधित अच्छे विचारों या उद्धरण को विषय वस्तु में सम्मिलित करना चाहिए।
5. निबंध की भाषा सरल, शुद्ध, सरस और विषय के अनुसार होनी चाहिए। विषयवस्तु लेखन करने के लिए उचित शैली का प्रयोग करना चाहिए।
6. निबंध लेखन के बाद उसे संपूर्ण निबंध को एक बार पढ़कर के देखना चाहिए तथा उसमें इच्छित संशोधन करना आवश्यक होता है।
7. निबंध का आकार विषय वस्तु के अनुसार होना चाहिए। इसका आकार एकदम बहुत बड़ा और बहुत छोटा नहीं करना चाहिए।
8. निबंध लेखन में अपने समस्त विचारों को पूर्णता के साथ स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। निबंध में क्रमबद्धता के साथ-साथ विचारों की संबद्धता का भी ध्यान रखना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही निबंध लेखन में व्याकरण का ध्यान रखते हुए उपर्युक्त स्थान पर विराम चिह्न आदि का प्रयोग करना चाहिए।
निबंध लेखन हिन्दी ( Rbse solution 12th class)
1. प्रस्तावना :- शिक्षा प्राप्त करना और मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। बिना शिक्षा के मनुष्य का विकास नहीं हो सकता है। शिक्षा की जब भी हम बात करते हैं तो आज भी सैकड़ो ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिससे शिक्षा में असमानता मिल जाएगी।
प्राचीन काल में नारी शिक्षा अर्थात बालिका शिक्षा का विशेष प्रबंध था। बालिकाओं के लिए गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। लेकिन कुछ वर्षों पूर्व तक बालिका शिक्षा की स्थिति सोचनीय बनी हुई थी। सरकार द्वारा बालिका शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं और अभियान चलाया जा रहे हैं लेकिन आज भी अनेक बालिकाएं शिक्षा से वंचित हैं।
2. बालिका शिक्षा की स्थिति व उसके कारण :– वर्तमान में भी भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति बहुत ही चिंताजनक बनी हुई है। लड़कों की तुलना में लड़कियों का विवाह जल्दी हो जाता है। घरेलू कामकाज में उनके द्वारा हाथ बंटाया जाता है, उनकी सुरक्षा का अभाव है।
छोटे भाई बहनों की देखभाल आदि के कारण से बालिकाओं की पढ़ाई में बाधा आती है। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होना और अभिभावक का अशिक्षित होना भी बालिकाओं की शिक्षा में बाधित बना हुआ है।
3. बालिका शिक्षा की आवश्यकता :- वर्तमान में बालिका शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकता समझ कर जोर दिया जा रहा है। बालिकाओं पर किसी भी देश का भविष्य निर्भर करता है क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर मां की भूमिका निभाती हैं और मां किसी भी परिवार की केंद्रीय इकाई होती है।
यदि मां को शिक्षा प्राप्त नहीं होती है तो वह एक स्वस्थ शिक्षित परिवार एवं उन्नत समाज के निर्माण में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसलिए बालिका के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है जिससे उनका नैतिक, व्यावहारिक, सामाजिक, बौद्धिक और कौशल विकास हो सके और वह आत्मनिर्भर बन सकें। जिससे अपने देश या समाज का विकास हो सके।
4. बालिका शिक्षा के लिए सरकार का प्रयास :– वर्तमान में सरकार द्वारा ऐसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। लोगों में जागरूकता फैलाने का काम विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं।
आम चुनावों में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है अर्थात सभी जगह पर सरकार द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान स्थान दिया गया है उनके माता-पिता तथा अभिभावक समझ सकें की बालिकाएं भी आगे चलकर बालकों की तरह कुछ कर सकती हैं।
यह सब सरकार की सुनियोजित योजनाओं का फल है। और आज हम देख रहे हैं समाज में बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव हुआ है और बालिका शिक्षा में काफी बढ़ोतरी हुई है।
5. उपसंहार :- कुछ वर्षों से बालिका की शिक्षा में देश में काफी प्रगति हुई है। और धीरे-धीरे समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न जैसी घटनाओं में भी काफी कमी हुई है और उनमें जागरूकता भी बढ़ी है।
लोगों को बालिका शिक्षा का महत्व समझाना बहुत जरूरी है। जिससे समाज का उचित विकास हो सके और हमको बालिका शिक्षा के लिए आम जनता को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए।
rbse solution 12th class
1. प्रस्तावना – पूरी दुनिया में वर्तमान में इंटरनेट का बहुत अधिक प्रसार हो चुका है। वर्तमान में कंप्यूटर के आविष्कार के साथ-साथ टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविजन, ईमेल, इंटरनेट आदि संचार साधनों का बहुत अधिक विस्तार हुआ है।
जनसंचार साधनों का असीमित विस्तार होने से जहां सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार हुआ है, वही संचार सुविधाओं में आश्चर्यजनक क्रांति आने से सूचना आदान-प्रदान अत्यंत सहज हो गया है। इंटरनेट का हर विभाग में और हर जगह सारी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जा रहा है।
2. इण्टरनेट ( internet) – इंटरनेट के उपयोग में संचार नेटवर्क कुछ कंप्यूटरों का समूह होता है। जिन्हें आपस में सूचनाओं तथा संसाधनों के सम आदान-प्रदान के लिए जोड़ा जाता है। इस प्रकार से पूरे विश्व में विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ दिया जाता है जिसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं।
अतः इंटरनेट कहीं नेटवर्कों का एक अंतरजाल होता है।अतः इंटरनेट संसार में व्याप्त सभी सूचनाओं, सूचना के भंडार को आपस में जोड़े रहता है तथा उन्हें किसी भी स्थान पर उपलब्ध करवाता है।
इस प्रकार सूचनाओं के ऐसे ऑनलाइन आदान-प्रदान को जिस माध्यम से पहुंचाया जाता है उसे हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि के माध्यम से किसी भी सूचना, मैसेज, ईमेल आदि का आदान-प्रदान करते हैं।
3. इण्टरनेट की रचना और कार्य – इंटरनेट के प्रचलन से पहले हमको किसी भी सूचना को प्राप्त करने में काफी समय लगता था। किसी व्यक्ति को कोई सूचना पहुंचानी होती थी, तो उसको पत्र लिखकर के डाक के माध्यम से भेजा जाता था, जिससे वह सूचना काफी समय बाद प्राप्त होती थी।
लेकिन इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी सूचना को तुरंत इस समय प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट दुनिया भर में फैला हुआ एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इसमें वे सेवा होती है जो किसी स्थान पर आफलाइन उपलब्ध होती हैं। इंटरनेट पर सभी ऐतिहासिक स्थल उपलब्ध रहते हैं जिनको एक वेबसाइट के माध्यम से अपलोड किया जाता है।
किसी भी स्थान की जानकारी हम इंटरनेट पर मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का समाचार पत्र घर बैठे पढ़ सकते हैं। इंटरनेट के प्रसार से तुरंत घटित होने वाली किसी भी सूचना की प्राप्ति तुरंत हो जाती है। इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थी अपनी किसी भी विषय पर शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं।
इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में प्रचलित किसी भी स्थान का स्वरूप और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से देश-विदेश में विभिन्न घटित होने वाली घटनाओं ऐतिहासिक जानकारी एवं विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं।
इंटरनेट के प्रचलन से सभी लोगों को बहुत ही अधिक लाभ हुआ है इससे विद्यार्थी घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इंटरनेट हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ है।
4. इंटरनेट की हानियां – इंटरनेट के प्रचलन से आज के संचार सेवाओं में बहुत ही अधिक सुविधा प्राप्त हुई है। इंटरनेट समाज में शिक्षा, संगठन और भागीदारी की दिशा में बहुत ही सकारात्मक कदम रहा है। घर बैठे हम किसी भी सूचना का आदान-प्रदान सरलता से कर सकते हैं।
लेकिन इसके साथ-साथ इसका दुरुपयोग भी बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। लोग इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन ठगी को अंजाम दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार के वायरस की लिंक भेजकर करके उनसे प्राइवेट डाटा चुरा लेते हैं तथा उसका दुरुपयोग किया जाता है।
इंटरनेट के माध्यम से साइबर अपराधियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है। वे दिन रात लोगों के साथ ठगी करने की फिराक में रहते हैं। इस प्रकार इंटरनेट का काफी दुरुपयोग भी हो रहा है। लेकिन लोगों को सावधानी के साथ इंटरनेट का प्रयोग करना चाहिए।
किसी भी प्रकार की लिंक को अपने साथ नहीं जोड़ना चाहिए। किसी अनजान मोबाइल नंबर आदि पर अपनी प्राइवेट सूचनाओं शेयर नहीं करनी चाहिए। इन साइबर अपराधों से बचकर रहना चाहिए।
5. उपसंहार – आज विज्ञान के योग में इंटरनेट एक ज्ञान का सागर के रूप में है। लेकिन इसके साथ-साथ इसमें काफी कूड़ा कचरा भी भरा पड़ा हुआ है। यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो ऐसे सागर से हम ज्ञानवान प्रगति के मोती हासिल कर सकते हैं।
यदि इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो हम कूड़े कचरे का अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार इंटरनेट का के हमेशा सदुपयोग करें और दुरुपयोग करने से हमेशा बचें और अपने साथियों को बचाए। इस प्रकार इंटरनेट के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू को ध्यान में रखते हुए हमें इसका उपयोग करना चाहिए।
rbse solution 12th class
1. प्रस्तावना :- दहेज शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी को भेंट या उपहार देना। प्राचीन काल से भारतवर्ष में दहेज का किसने किसी रूप में प्रचलन होता रहा है। उस समय विवाह संस्कार को मंगल कामनाओं का प्रतीक मान करके प्रेम पूर्वक विभिन्न प्रकार के दहेज का प्रचलन था।
कालांतर में इस शिष्टाचार रूढ़ि और प्रथाओं का प्रचलन और अधिक बढ़ता है गया और वर्तमान में यह दहेज प्रथा एक अभिशाप का रूप लेकर हमारे सामने प्रकट हुई है। आज के किसी भी प्रकार के विवाह संस्कार को करने से पहले दहेज की मांग को मुख्य पृष्ठ पर रखा जाता है।
2. दहेज प्रथा का अभिशाप – दहेज प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है। उस समय कन्या के विवाह केअवसर पर पिता अपनी संपत्ति का कुछ अंश उपहार के रूप में देता था। उस समय वही शुभकामना रहती थी की नव वर-वधू अपना नया घर अच्छी तरह से बसा सके तथा उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो।
इसी प्रथा को वर्तमान युग में लोग बड़ा चक्र चढ़कर के उपयोग कर रहे हैं लोग अपने बड़प्पन के लिए दहेज को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके दे रहे हैं जिससे गरीब इंसानों पर इसका बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इस गलत परंपरा के चलने से समाज में कन्याओं को एक भार के रूप में माना जाने लगा है।
वर्तमान में दहेज प्रथा के कारण समाज में अनेक परंपराएं चली हैं। बाल विवाह का प्रचलन बढ़ गया। कुछ लोग कन्या के जन्म को बहुत ही अशुभ मानते हैं। कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ा है। बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाने लगा।
3. दहेज प्रथा के दुष्परिणाम – वर्तमान समय में हमारे देश में दहेज प्रथा अपना विकराल रूप धारण कर चुकी है। आजकल वरपक्ष वाले अधिक से अधिक दहेज की मांग करते हैं । वे लड़के के जन्म से लेकर के पूरी पढ़ाई लिखाई विवाह का खर्च एवं उससे अधिक आभूषण, साजोसमान, गाड़ी, पैसा की मांग करते हैं।
जिससे गरीब लोगों पर इसका भौतिक गलत कामयाब घटना पड़ता है लोग कर्ज में डूब जाते हैं और सारी जिंदगी उसको चुकाने में निकल जाती है किसी को मनचाहा योजना मिलने से नंबरों को तंग किया जाता है और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है या उसको जला करके मार दिया जाता है।
दहेज के लिए लोग नववधू को घर से निकाल देते हैं और उसके साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं। इन बुराइयों के कारण दहेज प्रथा आज एक हमारे लिए अभिशाप बन चुकी है।
4. दहेज प्रथा में कानूनी और सामाजिक सुधार :– दहेज प्रथा के प्रचलन को बढ़ते देखकर के समय-समय पर समाज सुधारकों ने इस ओर ध्यान दिया है। भारत सरकार ने दहेज प्रथा में सुधार लाने के लिए दहेज प्रथा उन्मूलन का कानून बनाकर उसे सख्ती से लागू किया गया है।
अब दहेज देना व लेना कानूनन दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इस प्रथा में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं बहुत ही प्रशंसा के योग्य हैं। परंतु फिर भी वर्तमान में लोग इस प्रथा का त्याग नहीं कर रहे हैं लोग चोरी चुपके दहेज प्रथा को बढ़ावा दिए जा रहे हैं।
इसके लिए नवपीढी को जागृत होना आवश्यक होगा तथा इस कानून का सख्ती से पालन करते हुए दहेज प्रथा को जड़ से मिटाना होगा। जिससे इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं हो और दहेज प्रथा एक अभिशाप का रूप धारण न करें। इस प्रकार दहेज प्रथा में सुधार करके इसे जड़ से खत्म करके समाज को समृद्ध बनाया जा सकता है।
5. उपसंहार :- हमारे समाज में प्रारंभिक काल में दहेज का स्वरूप सरल था। लेकिन कालांतर में रूढ़ियों एवं लोग लालच के कारण यह सामाजिक अभिशाप बन गया है। सरकार ने दहेज प्रथा उन्मूलन कानून बनाकर इसको प्रथा को समाप्त करने के प्रयास किए हैं। परंतु इसमें जन जागरण की कमी के कारण अपेक्षित सुधार नहीं हो पाए हैं।
इस उक्ति को चरितार्थ बनाना होगा – दहेज लेना व देना मना है।
Hindi Gyan Sansar एक शैक्षणिक वेबसाइट है। यहां हम हिन्दी के लिए विस्तृत व्याकरण के संसाधन प्रदान करते हैं, साथ ही मनोविज्ञान (Psychology) के Notes व Questions-answers प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को स्पष्ट, रोचक ज्ञान प्रदान करना एवं उनकी समझ विकसित करना है।
Call Us on : 9461913326
Email : hindigyansansar24@gmail.com
© Hindi Gyan Sansar. All Rights Reserved. Website Developed By Media Tech Temple